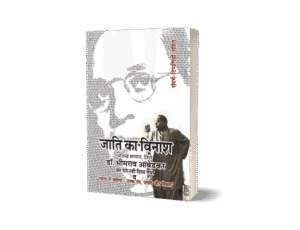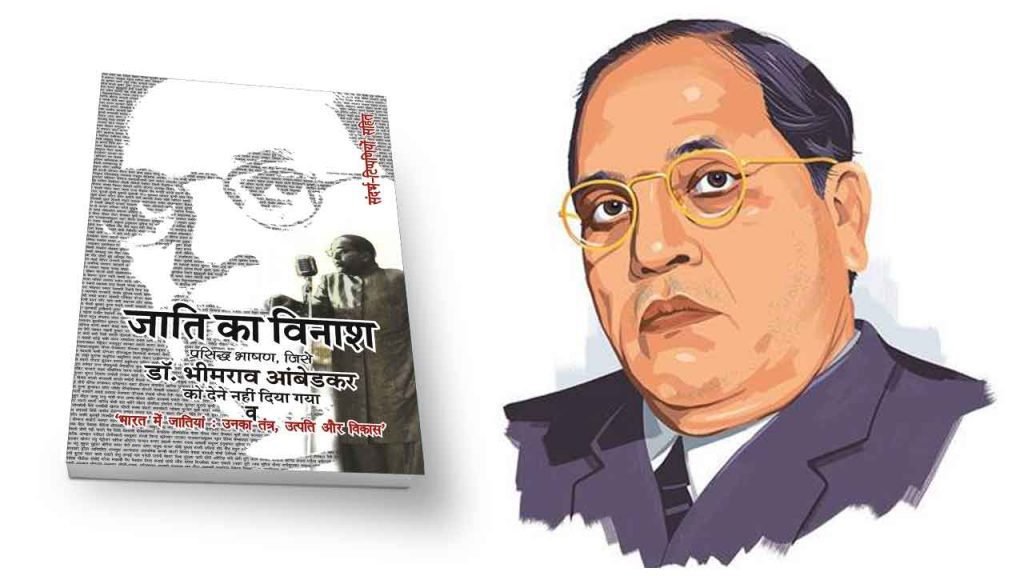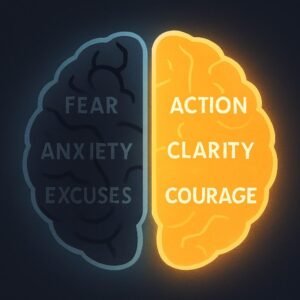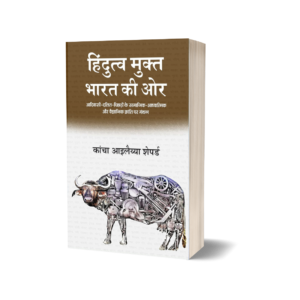डॉ. बी.आर. आंबेडकर के जाति का विनाश का संक्षिप्त विश्लेषण
सारांश
यह लेख डॉ. बी.आर. आंबेडकर की युगांतकारी कृति ‘जाति का विनाश‘ (Annihilation of Caste) के हिंदी संस्करण के मुख्य विषयों, तर्कों और ऐतिहासिक संदर्भ का एक व्यापक संश्लेषण प्रस्तुत करता है। मूल रूप से 1936 में लाहौर के ‘जात-पात तोड़क मंडल‘ के वार्षिक अधिवेशन के लिए एक अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया, यह व्याख्यान आयोजकों द्वारा इसके क्रांतिकारी और विवादास्पद विचारों, विशेष रूप से वेदों और शास्त्रों की सत्ता की अस्वीकृति और हिंदू धर्म छोड़ने के डॉ. आंबेडकर के निर्णय पर आपत्तियों के कारण कभी दिया नहीं जा सका। अधिवेशन रद्द होने के बाद, डॉ. आंबेडकर ने इसे अपने खर्च पर प्रकाशित किया, जिससे एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और सामाजिक बहस छिड़ गई, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए।
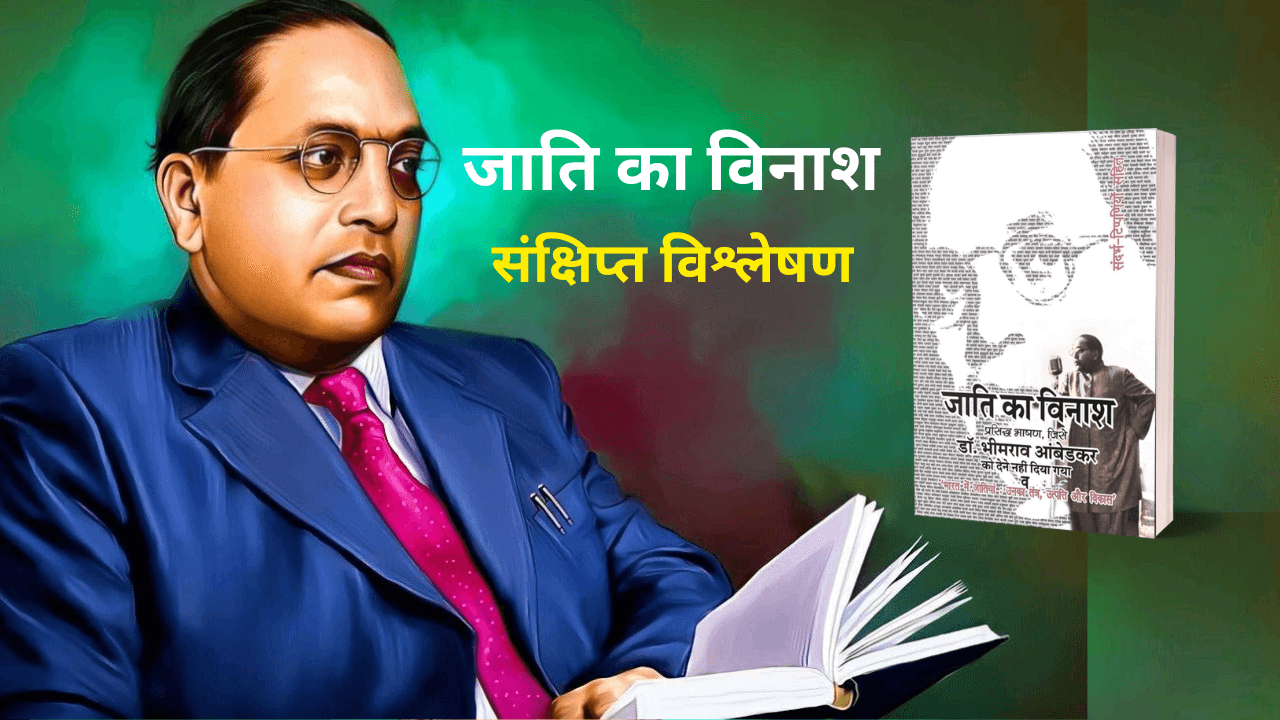
डॉ. आंबेडकर का केंद्रीय तर्क यह है कि जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का एक श्रेणीबद्ध, अस्वाभाविक और अन्यायपूर्ण विभाजन है। यह हिंदू समाज के नैतिक और सामाजिक पतन का मूल कारण है, जो सच्ची राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक एकजुटता और सार्वजनिक भावना के निर्माण को रोकता है। उन्होंने तर्क दिया कि जाति किसी भी सार्थक राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक सुधार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।
दस्तावेज़ में जाति के उन्मूलन के लिए प्रस्तावित विभिन्न उपायों, जैसे कि उप-जातियों को समाप्त करना, अंतर-जातीय भोज और आर्य समाज द्वारा प्रस्तावित ‘चातुर्वर्ण्य’ की पुनर्रचना की विस्तृत आलोचना शामिल है। डॉ. आंबेडकर इन सभी को अपर्याप्त मानते हैं। उनके अनुसार, जाति के विनाश का एकमात्र वास्तविक उपाय अंतर-जातीय विवाह है। हालांकि, वे इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदू अंतर-विवाह नहीं करते क्योंकि उनके धर्मग्रंथ (वेद, स्मृति, शास्त्र) इसकी मनाही करते हैं और जाति व्यवस्था को पवित्र और दैवीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।
इसलिए, डॉ. आंबेडकर का अंतिम निष्कर्ष यह है कि जाति को समाप्त करने के लिए, हिंदुओं को शास्त्रों के अधिकार और पवित्रता को पूरी तरह से अस्वीकार करना होगा। उनका आह्वान एक ऐसे नए सामाजिक-धार्मिक आधार के निर्माण का है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हो। अंत में, दस्तावेज़ में महात्मा गांधी के साथ हुई प्रसिद्ध बहस का सार भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें गांधी ने वर्ण-व्यवस्था का बचाव किया और डॉ. आंबेडकर ने उनके तर्कों का तीक्ष्ण खंडन किया।
——————————————————————————–
1. परिचय: एक भाषण जो दिया नहीं गया
डॉ. बी.आर. आंबेडकर की कृति ‘जाति का विनाश‘ वास्तव में एक पुस्तक के रूप में नहीं, बल्कि एक भाषण के रूप में लिखी गई थी। इसे लाहौर स्थित ‘जात-पात तोड़क मंडल’ के 1936 के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण के रूप में दिया जाना था। यह मंडल सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों का एक संगठन था जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज से जाति व्यवस्था को समाप्त करना था।
• विवाद का कारण: जब मंडल की स्वागत समिति ने भाषण का मसौदा देखा, तो वे इसकी विषय-वस्तु से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ अंशों पर उन्हें गंभीर आपत्ति थी। मुख्य आपत्तियाँ थीं:
1. डॉ. आंबेडकर द्वारा वेदों और शास्त्रों की सत्ता पर सीधा प्रहार।
2. उनकी यह घोषणा कि एक हिंदू के रूप में यह उनका अंतिम भाषण होगा, क्योंकि वे धर्म परिवर्तन का निर्णय ले चुके थे।
• अधिवेशन का रद्दीकरण: आयोजकों ने डॉ. आंबेडकर से इन विवादास्पद अंशों को हटाने का अनुरोध किया। हालांकि, डॉ. आंबेडकर ने अपने भाषण में किसी भी प्रकार के बदलाव से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि यह उनके विचारों की स्वतंत्रता और एक अध्यक्ष के कर्तव्य का मामला है। इस गतिरोध के परिणामस्वरूप, मंडल ने अधिवेशन को ही रद्द कर दिया।
• प्रकाशन और प्रतिक्रिया: भाषण देने का अवसर न मिलने पर, डॉ. आंबेडकर ने इसे 15 मई, 1936 को अपने खर्च पर एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवाया ताकि उनके विचार जनता तक पहुँच सकें। इस पुस्तिका ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया, विशेषकर महात्मा गांधी का, जिन्होंने अपने पत्र ‘हरिजन’ में इस पर दो आलोचनात्मक लेख लिखे। गांधी ने लिखा, “कोई भी सुधारक इस व्याख्यान की उपेक्षा नहीं कर सकता… डॉ. आंबेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती हैं।” इसके जवाब में डॉ. आंबेडकर ने एक विस्तृत प्रत्युत्तर लिखा, जिसे बाद में पुस्तक के दूसरे संस्करण में “महात्मा को जवाब” शीर्षक से जोड़ा गया।
जाति का विनाश पुस्तक खरीदने के लिए यहाँ क्लिक करें
2. जाति व्यवस्था का विश्लेषण
डॉ. आंबेडकर जाति व्यवस्था का एक बहुआयामी और विनाशकारी सामाजिक संरचना के रूप में विश्लेषण करते हैं।
जाति श्रम का नहीं, श्रमिकों का विभाजन है
जाति व्यवस्था के समर्थक अक्सर यह तर्क देते हैं कि यह केवल ‘श्रम विभाजन’ का एक रूप है, जो हर सभ्य समाज में आवश्यक है। डॉ. आंबेडकर इस तर्क को सिरे से खारिज करते हैं:
• श्रमिकों का विभाजन: यह केवल कार्यों का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का एक-दूसरे से अलग-थलग समूहों में अस्वाभाविक विभाजन है।
• श्रेणीबद्ध असमानता: यह एक ऐसी ऊँच-नीच की व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों को एक-दूसरे के ऊपर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह किसी अन्य देश के श्रम विभाजन में नहीं पाया जाता।
• पेशा का पूर्व-निर्धारण: यह किसी व्यक्ति की नैसर्गिक क्षमताओं या रुचि के बजाय उसके जन्म के आधार पर उसका पेशा पूर्व-निर्धारित कर देता है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक दक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है।
• गतिशीलता का अभाव: यह व्यक्तियों को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होती है, क्योंकि व्यक्ति बदलती औद्योगिक परिस्थितियों के अनुकूल खुद को नहीं ढाल पाता।
जाति और सामाजिक एकता का अभाव
डॉ. आंबेडकर के अनुसार, जाति ने हिंदुओं को एक सच्चा समाज या राष्ट्र बनने से रोका है।
• हिंदू समाज एक मिथक है: हिंदू समाज का अस्तित्व नहीं है; यह केवल जातियों का एक समुच्चय है। प्रत्येक जाति केवल अपने अस्तित्व के प्रति सचेत है और अन्य जातियों से खुद को अलग रखने का प्रयास करती है।
• “साझा चेतना” का अभाव: हिंदुओं में एक-दूसरे के प्रति अपनेपन या सामुदायिक भावना की कमी है। उनमें केवल अपनी जाति के सदस्य होने की चेतना है।
• समाज-विरोधी भावना: जाति व्यवस्था का सबसे निकृष्टतम लक्षण यह है कि यह एक जाति में दूसरी जाति के प्रति घृणा और द्वेष की भावना पैदा करती है। यह भावना केवल जातियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उप-जातियों के संबंधों में भी व्याप्त है।
• संगठन में बाधा: जाति हिंदुओं को संगठित होने से रोकती है। उनमें आपसी सहयोग, विश्वास और बंधुत्व की भावना का अभाव है, जिसके कारण वे ऐतिहासिक रूप से कमजोर और कायर बने रहे हैं।
जाति और नस्लीय शुद्धता का मिथक
जाति का एक और बचाव यह कहकर किया जाता है कि इसका उद्देश्य नस्लीय शुद्धता और रक्त की पवित्रता बनाए रखना है। डॉ. आंबेडकर इस तर्क को अवैज्ञानिक और तथ्यों के विपरीत बताते हैं:
• नस्लीय मिश्रण: मानव-वैज्ञानिकों का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि भारत में कोई भी जाति या वर्ग ऐसा नहीं है जिसमें विदेशी रक्त का मिश्रण न हुआ हो, यहाँ तक कि ब्राह्मणों में भी।
• जाति नस्ल नहीं है: पंजाब के ब्राह्मण और मद्रास के ब्राह्मण में या पंजाब के ब्राह्मण और पंजाब के चमार में नस्लीय रूप से कोई खास अंतर नहीं है। जाति एक ही नस्ल के लोगों का सामाजिक विभाजन है, न कि विभिन्न नस्लों का।
• अवैज्ञानिक आधार: सुजनन विज्ञान (Eugenics) के आधार पर जाति का बचाव करना निरर्थक है, क्योंकि जाति केवल विभिन्न जातियों के बीच विवाह को रोकती है; यह किसी विशेष जाति के भीतर सर्वश्रेष्ठ के चयन का कोई सकारात्मक तरीका प्रदान नहीं करती।
3. सुधार के मार्ग में जाति एक बाधा
डॉ. आंबेडकर का तर्क है कि जाति व्यवस्था हर प्रकार के सुधार – राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक – के लिए एक शक्तिशाली अवरोधक है।
राजनीतिक सुधार
• डॉ. आंबेडकर का मानना है कि राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार एक अनिवार्य शर्त है। एक विभाजित और अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचना एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था को जन्म नहीं दे सकती।
• वे तर्क देते हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि राजनीतिक क्रांतियाँ हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद हुई हैं। उन्होंने यूरोप में लूथर के सुधार आंदोलन, इंग्लैंड में प्यूरिटनिज्म और भारत में बुद्ध की क्रांति के बाद चंद्रगुप्त के उदय, और महाराष्ट्र के संतों के बाद शिवाजी के उदय का उदाहरण दिया।
• उनका कहना है कि जब तक समाज में मन और आत्मा की मुक्ति नहीं होती, तब तक राजनीतिक विस्तार संभव नहीं है।
आर्थिक सुधार और समाजवाद
डॉ. आंबेडकर भारतीय समाजवादियों की इस धारणा की आलोचना करते हैं कि केवल आर्थिक सुधार (संपत्ति की समानता) से सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
• शक्ति के अन्य स्रोत: उनका तर्क है कि संपत्ति ही शक्ति का एकमात्र स्रोत नहीं है। धर्म और सामाजिक स्थिति भी शक्ति के शक्तिशाली स्रोत हैं, विशेषकर भारत में।
• सर्वहारा की एकता असंभव: जाति व्यवस्था भारत के सर्वहारा (श्रमिक वर्ग) को विभाजित करती है। जब तक श्रमिक अपनी जातिगत पहचान (ऊँच-नीच, शुद्ध-अशुद्ध) को नहीं छोड़ते, वे अमीरों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते।
• क्रांति के बाद की चुनौती: यदि समाजवादी क्रांति करने में सफल हो भी जाते हैं, तो उन्हें जाति द्वारा उत्पन्न समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। जाति एक ऐसा राक्षस है जो हर रास्ते में बाधा डालेगा।
4. जाति का विनाश के प्रस्तावित उपाय और उनकी सीमाएँ
डॉ. आंबेडकर जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रचलित विभिन्न सुधारवादी दृष्टिकोणों का विश्लेषण करते हैं और उन्हें अपर्याप्त पाते हैं।
• उप-जातियों का उन्मूलन: कुछ सुधारकों का मानना है कि पहले उप-जातियों को समाप्त करना चाहिए, जिससे बड़ी जातियों का विलय आसान हो जाएगा। डॉ. आंबेडकर इसे एक भ्रम मानते हैं। उनका तर्क है कि इससे जातियाँ और भी अधिक मजबूत और शक्तिशाली हो सकती हैं।
• अंतर-जातीय भोज: इसे भी वे एक अपर्याप्त उपचार मानते हैं। उनका अनुभव है कि कई जातियों में सह-भोज प्रचलित है, लेकिन इससे जाति की भावना या चेतना समाप्त नहीं हुई है।
• चातुर्वर्ण्य की पुनर्रचना: वे आर्य समाज के उस आदर्श की तीखी आलोचना करते हैं जो हिंदू समाज को जन्म के बजाय गुण के आधार पर चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) में पुनर्गठित करना चाहता है।
◦ अव्यावहारिक: लोगों को चार स्पष्ट वर्गों में वर्गीकृत करना असंभव है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है।
◦ हानिकारक: यह शूद्रों के लिए सबसे बुरी व्यवस्था होगी क्योंकि यह उन्हें शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति के अधिकार से वंचित करके उनका स्थायी निम्नीकरण कर देगी।
◦ ऐतिहासिक विफलता: यह व्यवस्था अतीत में भी संघर्षों (ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच) के कारण विफल रही है। इसे बनाए रखने के लिए एक कठोर दंड विधान की आवश्यकता होगी, जैसा कि राम द्वारा शंबूक की हत्या और मनुस्मृति के कानूनों से स्पष्ट है।
5. आंबेडकर का प्रस्तावित समाधान: शास्त्रों का विनाश
उपरोक्त उपायों को खारिज करने के बाद, डॉ. आंबेडकर जाति के विनाश के लिए अपना मौलिक और क्रांतिकारी समाधान प्रस्तुत करते हैं।
• वास्तविक उपाय: अंतर-जातीय विवाह: उनके अनुसार, “जाति को तोड़ने का असली उपचार अंतर-जातीय विवाह है। और कुछ भी जाति के विलयन का काम नहीं कर सकेगा।” केवल रक्त का सम्मिश्रण ही अपनेपन और रिश्तेदारी की भावना पैदा कर सकता है जो जाति की अलगाववादी भावना को नष्ट कर सकती है।
• मुख्य बाधा: धार्मिक मान्यताएँ: लोग अंतर-जातीय विवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र इसे प्रतिबंधित करते हैं। हिंदुओं का जाति का पालन करना उनकी अमानवीयता के कारण नहीं, बल्कि उनकी गहरी धार्मिकता के कारण है।
• अंतिम लक्ष्य: शास्त्रों के अधिकार को नष्ट करना: इसलिए, वास्तविक शत्रु वे लोग नहीं हैं जो जाति का पालन करते हैं, बल्कि वे शास्त्र हैं जो उन्हें जाति-आधारित धर्म की शिक्षा देते हैं। डॉ. आंबेडकर का निष्कर्ष है:
“आपको वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगा देना होगा… आपको श्रुतियों और स्मृतियों के धर्म को नष्ट कर देना होगा। और कोई भी उपाय काम नहीं करेगा।”
आदर्श समाज: स्वतंत्रता, समता और बंधुता
जाति-आधारित समाज के स्थान पर, डॉ. आंबेडकर एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जो स्वतंत्रता, समता (समानता) और बंधुता पर आधारित हो।
• बंधुता (Fraternity): इसका दूसरा नाम लोकतंत्र है। यह केवल शासन की एक शैली नहीं, बल्कि साझा अनुभवों और अपने साथियों के प्रति सम्मान की भावना है।
• स्वतंत्रता (Liberty): इसमें केवल जीवन और संपत्ति का अधिकार ही नहीं, बल्कि अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता भी शामिल होनी चाहिए।
• समता (Equality): यह स्वीकार करते हुए कि सभी मनुष्य समान नहीं हैं, वे तर्क देते हैं कि इसे एक नियंत्रक सिद्धांत के रूप में अपनाना होगा ताकि जन्म, शिक्षा और विरासत जैसे विशेषाधिकारों के बजाय योग्यता को अवसर मिले।
6. गांधी-आंबेडकर बहस
डॉ. आंबेडकर के भाषण के प्रकाशन के बाद महात्मा गांधी ने ‘हरिजन’ में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके जवाब में डॉ. आंबेडकर ने एक विस्तृत प्रत्युत्तर लिखा।
विषय |
महात्मा गांधी का पक्ष |
डॉ. बी.आर. आंबेडकर का प्रत्युत्तर |
|
शास्त्र
|
शास्त्रों की व्याख्या विद्वानों द्वारा नहीं, बल्कि संतों द्वारा की जानी चाहिए। प्रामाणिक शास्त्र जाति और अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करते।
|
आम जनता विद्वानों और संतों की व्याख्याओं में अंतर नहीं करती; वे वही मानती है जो उन्हें सिखाया गया है। संतों ने कभी जाति व्यवस्था पर मौलिक प्रहार नहीं किया।
|
|
वर्ण बनाम जाति
|
वर्ण और जाति अलग-अलग हैं। वर्ण पैतृक पेशे का पालन करने का नियम है, जो समाज में स्थिरता लाता है और इसमें ऊँच-नीच का भाव नहीं है।
|
गांधी का ‘वर्ण’ जाति का ही दूसरा नाम है, क्योंकि दोनों का आधार पैतृक पेशा है। यह एक अव्यावहारिक और अनैतिक आदर्श है। गांधी स्वयं अपने पैतृक पेशे का पालन नहीं करते।
|
|
धर्म का मूल्यांकन
|
किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम नमूनों से नहीं, बल्कि उसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों (संतों) से किया जाना चाहिए।
|
यह तर्क इस सवाल का जवाब नहीं देता कि हिंदू धर्म में निकृष्ट लोगों की संख्या इतनी अधिक और उत्कृष्ट (संतों) की संख्या इतनी कम क्यों है। इसका कारण धर्म के गलत आदर्श हैं।
|
|
सुधार का मार्ग
|
सवर्ण हिंदुओं के व्यक्तिगत चरित्र में सुधार और उनके द्वारा शास्त्रों की उदार व्याख्या से समस्या हल हो सकती है।
|
व्यक्तिगत चरित्र एक ऐसी व्यवस्था को नहीं बदल सकता जो एक मौलिक रूप से गलत संबंध (ऊँच-नीच) पर आधारित हो। एक अच्छा हिंदू होना संभव नहीं है जब तक जाति मौजूद है।
|
|
हिंदुत्व का सार
|
हिंदुत्व का सार एक ईश्वर में विश्वास और अहिंसा के नियम में निहित है, न कि जाति में।
|
गांधी अपने रुख में विरोधाभासी हैं। कभी वे कहते हैं कि वर्ण हिंदुत्व का अभिन्न अंग है, और कभी इसे सार से बाहर कर देते हैं।
|
डॉ. आंबेडकर का अंतिम निष्कर्ष यह था कि हिंदू समाज को एक नैतिक पुनरुत्थान की आवश्यकता है, लेकिन इसके नेता, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल हैं, इस कार्य के लिए अयोग्य हैं क्योंकि वे समाज की बुनियाद का पुनरीक्षण करने से डरते हैं और सोचने के बजाय संतों का अंधानुकरण करना पसंद करते हैं।
——————————————————————————–